श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 7 (Bhagavad Gita Chapter 3 Verse 7 in Hindi): भगवद्गीता का प्रत्येक श्लोक गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है और हमें जीवन की सच्ची दिशा प्रदान करता है। अध्याय 3, जिसे ‘कर्मयोग’ कहा जाता है, विशेष रूप से कर्म और उसके महत्व को दर्शाता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म से विमुख होना या मात्र संन्यास धारण करना श्रेष्ठता की निशानी नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। इसी संदर्भ में श्लोक 3.7 में कर्मयोग का महत्व प्रतिपादित किया गया है।
श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 7 (Bhagavad Gita Chapter 3 Verse 7)
श्लोक 3 . 7
Bhagavad Gita Chapter 3 Verse-Shloka 7
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेSर्जुन |
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते || ७ ||
गीता अध्याय 3 श्लोक 7 अर्थ सहित (Gita Chapter 3 Verse 7 in Hindi with meaning)

श्लोक 3.7: कर्मयोगी की श्रेष्ठता
संस्कृत श्लोक:
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेSर्जुन |
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते || ७ ||
शब्दार्थ:
- यः – जो
- तु – लेकिन
- इन्द्रियाणि – इन्द्रियों को
- मनसा – मन के द्वारा
- नियम्य – वश में करके
- आरभते – प्रारम्भ करता है
- अर्जुन – हे अर्जुन
- कर्मेन्द्रियैः – कर्मेन्द्रियों से
- कर्म-योगम् – भक्ति
- असक्तः – अनासक्त
- सः – वह
- विशिष्यते – श्रेष्ठ है
भावार्थ
इस श्लोक में श्रीकृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन से अपनी इन्द्रियों को नियंत्रित करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग का पालन करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह है कि केवल बाहरी रूप से संन्यास धारण करना या इन्द्रिय भोगों से बचना ही योग नहीं है, बल्कि मन और कर्म का संयमित उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना सच्चा योग है।
तात्पर्य: कर्म में ही मुक्ति का रहस्य
श्रीकृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि केवल बाह्य रूप से योगी या संन्यासी बनना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों में लिप्त होते हुए भी मन को नियंत्रित कर निष्काम भाव से कर्म करता है, तो वह अधिक श्रेष्ठ है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति मात्र दिखावे के लिए योगी बनता है लेकिन मन से विषय-वासना में लिप्त रहता है, वह पाखंडी कहलाता है।
मुख्य बिंदु:
✔ निष्काम कर्म ही सच्चा योग है।
✔ बाह्य संन्यास से अधिक महत्वपूर्ण है मन का संयम।
✔ दिखावे की भक्ति और पाखंड से बचना चाहिए।
✔ कर्म के बंधन से मुक्ति केवल अनासक्त भाव से संभव है।
कर्मयोग: एक संतुलित जीवन जीने की कला
भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने कर्मयोग को एक ऐसे मार्ग के रूप में बताया है जो सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। व्यक्ति यदि पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ कार्य करता है, तो वह कर्म के बंधन से मुक्त रहता है।
कर्मयोगी और पाखंडी में अंतर
एक गाँव में दो साधु रहते थे—महादेव बाबा और साधु गिरीश। दोनों का रहन-सहन एक जैसा था, परंतु उनकी जीवनशैली और कर्म करने की भावना में बड़ा अंतर था।
साधु गिरीश (पाखंडी योगी)
साधु गिरीश ने अपना सिर मुँडा रखा था, भगवा वस्त्र धारण किए थे, और हमेशा भक्ति व त्याग की बातें करते थे। वे गाँव वालों को प्रवचन देते कि “संसार माया है, इससे दूर रहो, त्याग ही मोक्ष का मार्ग है।” लेकिन अंदर ही अंदर वे धन और सम्मान के लालची थे।
- वे अपने प्रवचनों से लोगों से चढ़ावा और दान माँगते थे।
- उनके शिष्यों को कठिन नियमों का पालन करने की सलाह देते थे, लेकिन स्वयं उन नियमों का पालन नहीं करते थे।
- वे बाहरी रूप से योगी थे, लेकिन भीतर से सांसारिक सुखों में लिप्त रहते थे।
महादेव बाबा (सच्चे कर्मयोगी)
महादेव बाबा, दूसरी ओर, साधारण कपड़े पहनते थे, कोई बड़ा दावा नहीं करते थे और गाँव के लोगों के साथ ही खेतों में काम करते थे। वे मानते थे कि “सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में बैठने से नहीं, बल्कि अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करने से होती है।”
- वे खेतों में मेहनत करते और अपने श्रम से जो कमाते, उसे ज़रूरतमंदों में बाँट देते।
- वे किसी से दान नहीं माँगते, बल्कि स्वयं ईमानदारी से जीवनयापन करते।
- वे भक्ति और साधना के साथ कर्म को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते थे।
अंतर और शिक्षा
साधु गिरीश केवल बाहरी रूप से संन्यासी थे लेकिन भीतर से सांसारिक वासनाओं में लिप्त। उन्होंने भक्ति को दिखावे का साधन बना लिया था। दूसरी ओर, महादेव बाबा सच्चे कर्मयोगी थे, जिन्होंने अपने कर्म के माध्यम से ईश्वर की भक्ति की।
👉 सच्चा योगी वह है जो मन को नियंत्रित रखकर कर्म करता है, न कि वह जो केवल दिखावे के लिए संन्यासी बनता है।
👉 बाहरी वेशभूषा से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धता और निष्काम भाव से कर्म करना।
गृहस्थ जीवन में भी कर्मयोग संभव है
बहुत से लोग यह मानते हैं कि केवल संन्यास ग्रहण करके ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति भी ईश्वर की भक्ति और सेवा में लगे रहकर कर्मयोग के मार्ग पर चल सकता है।
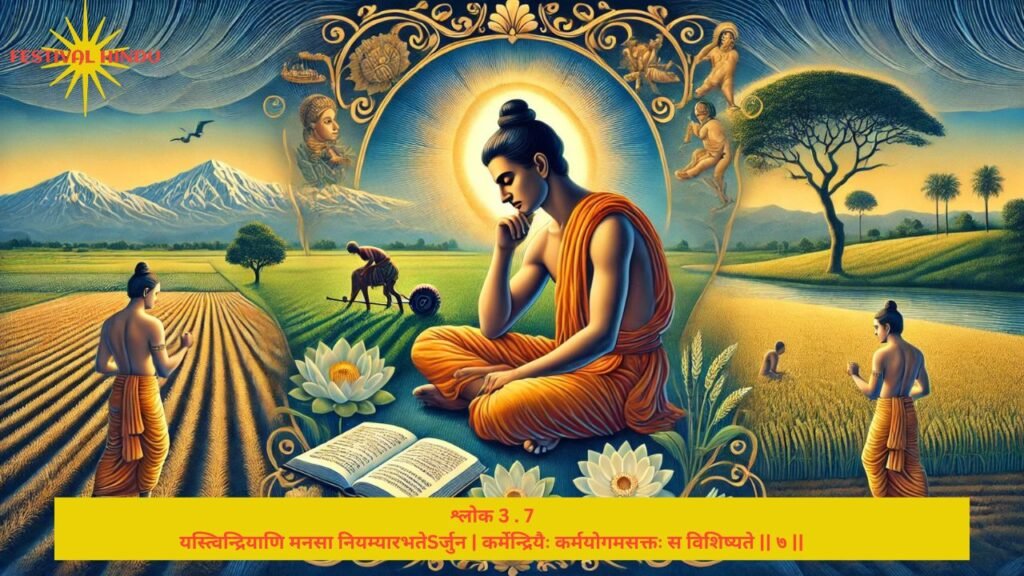
गृहस्थ जीवन में कर्मयोग अपनाने के तरीके:
- अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करने की भावना विकसित करें।
- स्वार्थरहित सेवा करें और परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करें।
- नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण और ध्यान करें।
- लोभ, अहंकार, और वासनाओं से बचें।
- ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन यापन करें।
कर्मयोग का वास्तविक उद्देश्य
कर्मयोग केवल कार्य करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ती है। इस मार्ग को अपनाने से व्यक्ति जीवन के सुख-दुख, लाभ-हानि, जय-पराजय में समान भाव रखता है।
श्रीकृष्ण के अनुसार कर्मयोगी के लक्षण:
✔ इन्द्रियों पर नियंत्रण रखता है।
✔ कार्य करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता।
✔ फल की चिंता किए बिना कर्म करता है।
✔ स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है।
✔ दिखावे से दूर रहता है और पाखंड नहीं करता।
निष्कर्ष
श्रीकृष्ण ने कर्मयोग को ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है। केवल कर्म से दूर भागना या संन्यास लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन को संयमित रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ा रहता है, वही वास्तविक कर्मयोगी है। इस प्रकार, हम सभी को निष्काम भाव से कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम कर्म के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ सकें।
मुख्य सारांश:
✅ कर्मयोग = कर्म + भक्ति
✅ संन्यास से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म में अनासक्ति।
✅ निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है।
✅ दिखावे और पाखंड से बचकर ईमानदारी से कर्म करें।
✅ गृहस्थ जीवन में भी कर्मयोग अपनाया जा सकता है।
“कर्मयोग अपनाएं और जीवन को सार्थक बनाएं!” 🚩
Resources : श्रीमद्भागवत गीता यथारूप – बक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, गीता प्रेस

