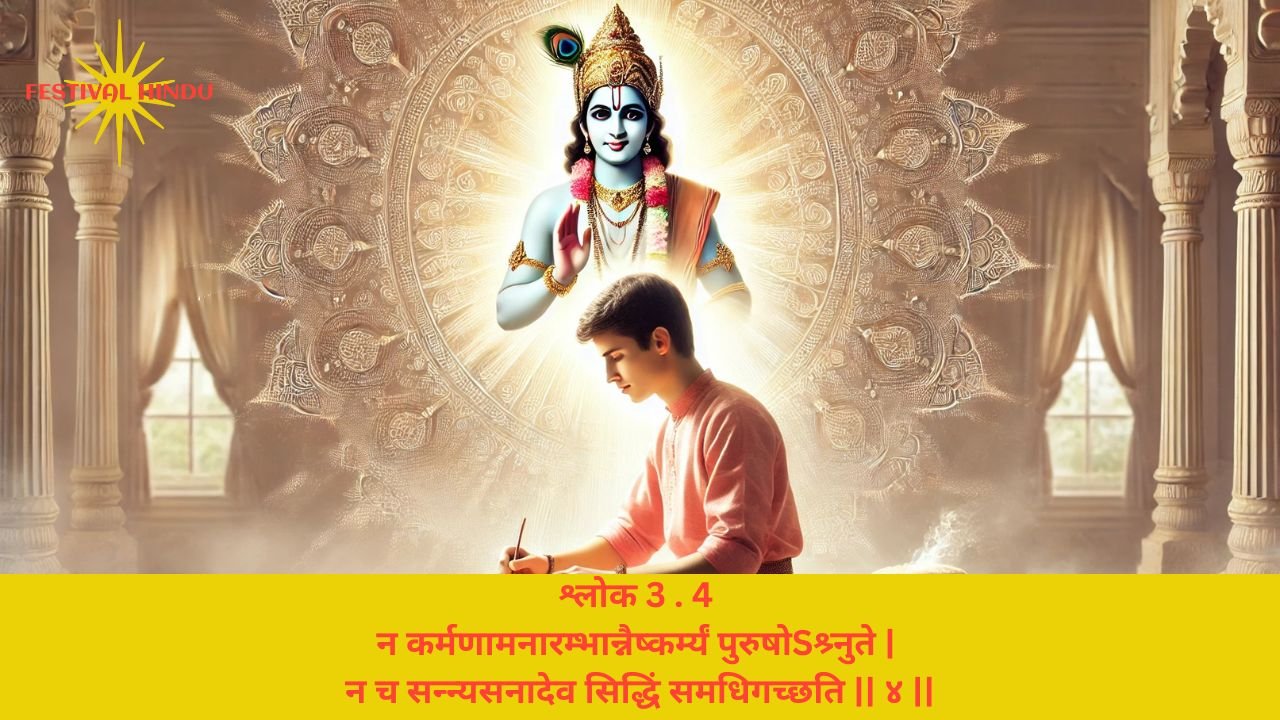श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 4 (Bhagavad Gita Chapter 3 Verse 4 in Hindi): भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जिसे “कर्मयोग” कहा जाता है, जीवन में कर्म की अनिवार्यता को समझाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मनुष्य केवल कर्म का त्याग कर देने मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। कई लोग यह सोचते हैं कि संसारिक कार्यों से दूर रहकर या संन्यास धारण कर लेने से वे जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन गीता में श्रीकृष्ण इस धारणा को नकारते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि मोक्ष का मार्ग केवल कर्म के निषेध से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण से किए गए कर्मों से ही प्राप्त होता है।
कर्म और संन्यास के इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमें श्लोक 3.4 का गहराई से अध्ययन करना होगा। इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल कर्म से विमुख होकर मुक्ति नहीं पा सकता, और न ही मात्र संन्यास से उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है।
श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 4 (Bhagavad Gita Chapter 3 Verse 4)
श्लोक 3 . 4
Bhagavad Gita Chapter 3 Verse-Shloka 4
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोSश्र्नुते |
न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति || ४ ||
गीता अध्याय 3 श्लोक 4 अर्थ सहित (Gita Chapter 3 Verse 4 in Hindi with meaning)
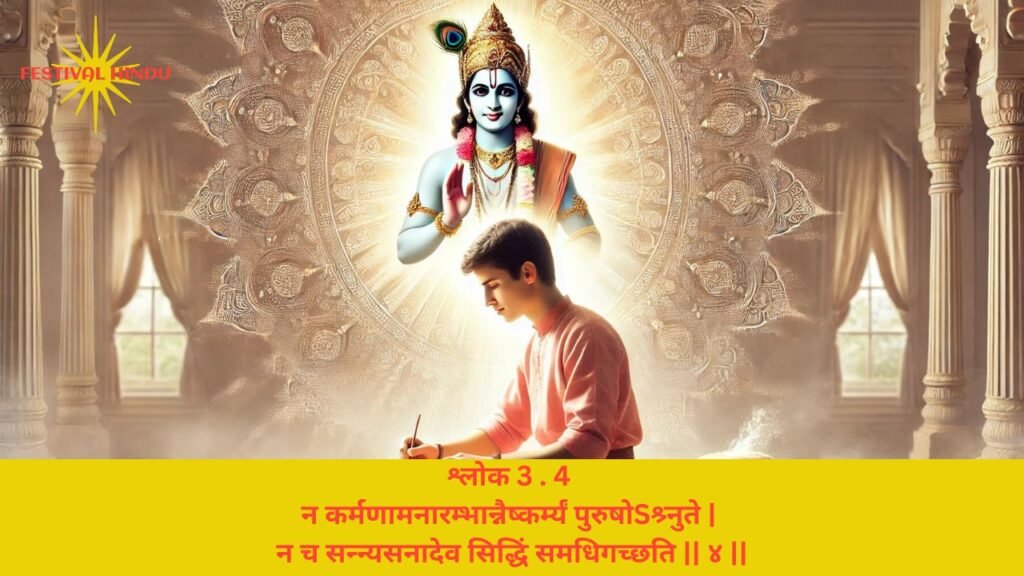
श्लोक 3.4
संस्कृत:
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोSश्र्नुते |
न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति || ४ ||
शब्दार्थ:
- न – नहीं
- कर्मणाम् – नियत कर्मों के
- अनाराम्भात् – न करने से
- नैष्कर्म्यम् – कर्मबन्धन से मुक्ति
- पुरुषः – मनुष्य
- अश्र्नुते – प्राप्त करता है
- न – नहीं
- च – भी
- संन्यसनात् – त्याग से
- एव – केवल
- सिद्धिम् – सफलता
- समधिगच्छति – प्राप्त करता है
अर्थ:
न तो कर्मों को न करने से मनुष्य कर्मबंधन से मुक्त हो सकता है और न ही केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
भावार्थ और व्याख्या
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण यह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल निष्क्रियता अपनाकर मुक्ति नहीं पा सकता। इसी प्रकार केवल संन्यास धारण करने से भी सिद्धि संभव नहीं है। यह धारणा कि संसारिक कर्तव्यों से विमुख होकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, गीता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह चाहे जितना भी शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहे, उसके विचार कभी रुकते नहीं हैं। वह निरंतर सोचता रहता है, चिंतन करता है, और यह मानसिक प्रक्रिया भी एक प्रकार का कर्म ही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति केवल बाहरी रूप से कर्मों को रोककर नैष्कर्म्य (कर्मफल से मुक्ति) को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीकृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि मन की शुद्धि के बिना संन्यास भी एक निरर्थक प्रक्रिया है।
कर्म और संन्यास का सही अर्थ
भगवद गीता में कर्मयोग को आत्मा की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि केवल संन्यास धारण कर लेना ही मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक संन्यास भी फलदायी नहीं होगा। वास्तव में, सच्चा संन्यास वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन किसी भी फल की अपेक्षा नहीं रखता।
आज के समाज में भी कई लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का एकमात्र मार्ग सांसारिक जीवन का त्याग करना है। वे सोचते हैं कि केवल तपस्या, ध्यान और भौतिक वस्तुओं के त्याग से वे ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन श्रीकृष्ण इस विचारधारा का खंडन करते हैं और बताते हैं कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। जब तक मनुष्य अपने कर्तव्यों को नहीं निभाएगा, तब तक उसकी आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है।
कर्मयोग और निष्काम कर्म का महत्व
गीता में निष्काम कर्म को सर्वोच्च बताया गया है। निष्काम कर्म का अर्थ है – कर्म करना लेकिन बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। जब कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, तो वह कर्मबंधन में फँस जाता है। लेकिन जब वही कार्य बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है, तो वह ईश्वर की सेवा बन जाता है।
श्रीकृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल संन्यास धारण करके आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। बाहरी संन्यास केवल एक आडंबर हो सकता है, यदि मन अशुद्ध बना रहे। मन की प्रवृत्ति ही उसे भटकाने वाली होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल भौतिक रूप से संसार का त्याग कर ले, लेकिन उसका मन अब भी सांसारिक इच्छाओं से भरा हो, तो वह वास्तविक संन्यासी नहीं हो सकता।
इसलिए, गीता में कर्मयोग को सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है। कर्मयोग में व्यक्ति अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित कर देता है और उनकी इच्छा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जब कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं, तब वे मनुष्य को कर्मबंधन से मुक्त करते हैं।
श्लोक 3.4 से हमें क्या सीखने को मिलता है?
श्रीकृष्ण के इस उपदेश से हमें यह समझ में आता है कि कर्म से विमुख रहना या केवल संन्यास धारण कर लेना, मोक्ष का सही मार्ग नहीं है। जीवन में कर्तव्यों का निर्वाह करना आवश्यक है, लेकिन हमें कर्म के फल की आसक्ति से बचना चाहिए।
आज के समय में भी कई लोग अपने कार्यों से बचने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है – कर्मों का त्याग करना और केवल ध्यान तथा पूजा में लीन रहना। लेकिन गीता का संदेश बिल्कुल अलग है। श्रीकृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो संसार में रहते हुए भी निष्काम कर्म करता है और अपने कार्यों को भगवान की सेवा मानता है।
इस श्लोक से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मन की शुद्धि के बिना कोई भी व्यक्ति संन्यास धारण करके सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बाहरी संन्यास का कोई महत्व नहीं है यदि मन में वासनाएँ बनी रहें। केवल वैराग्य धारण करने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक मन और बुद्धि को शुद्ध नहीं किया जाता।
निष्कर्ष
श्लोक 3.4 का मुख्य संदेश यह है कि निष्क्रियता से मोक्ष संभव नहीं है और केवल संन्यास धारण कर लेने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। सच्ची सिद्धि तब मिलती है जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है और कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। कर्मयोग का सार यही है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाए, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहे।
भगवद गीता का यह संदेश आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों वर्ष पहले था। यदि हम इस श्लोक के गूढ़ अर्थ को समझें और अपने जीवन में इसे अपनाएँ, तो हम निश्चित रूप से आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कर्म ही धर्म है, और निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। 🚩
Resources : श्रीमद्भागवत गीता यथारूप – बक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, गीता प्रेस